मानव शरीर इस निखिल ब्रह्माण्ड की सबसे सुन्दर कृति है। मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव शरीर में निखिल ब्रह्माण्ड समहित है। सामान्य मानव जब पतन के मार्ग में पहुंच जाता है, तो बहुत ही दीन-हीन, असमर्थ, असहाय, मानसिक विकलांग और अपंग होकर उस अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वह स्वयं के जीवन का भी संचालन नहीं कर पाता। वहीं यह मनुष्य उच्चता की ओर बढ़ता है तथा मानवीय मूल्यों को स्थापित करता हुआ धर्मपथ पर बढ़कर अष्टांग योग के मार्ग में चलता है और अपनी समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध करके समाधि की अवस्था वैराग्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह अपनी पूर्ण आत्मचेतना को जाग्रत् करके अलौकिक दिव्यशक्तियों का मालिक बनता हुआ, अनन्त लोकों से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। अपने अनुसार कुछ भी करने के लिए सामथ्र्यवान् बन जाता है। साथ ही वह प्रकृतिसत्ता का एक सहायक अंग बनकर मानव से महामानव बन जाता है। ऋषित्व पद को प्राप्त करके वह दिव्यधाम का वासी बनता है, जो मानव जीवन का अंतिम पड़ाव और लक्ष्य है।
शून्य से शिखर तक की इस यात्रा को तय करने के लिए हमें अपने तन-मन और बुद्धि को स्वस्थ निर्मल चेतनावान् बनाते हुए बढऩा पड़ता है। मनुष्य को अपनी जीवनचर्या को एक व्यवस्थित स्वरूप देना पड़ता है। आहार-विहार-विचारों को व्यवस्थित रखकर आगे बढऩा पड़ता है। अष्टांग येाग में इस पूरी यात्रा को आठ महत्त्वपूर्ण अंगों में बांटा गया है, जो क्रमश:- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। इन आठों अंगों में पूर्णतया निष्ठा-विश्वास और समर्पण के साथ चलने पर ही हमें पूर्णत्व का लाभ प्राप्त होता है। यदि मनुष्य साधना की चरम अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, तो अष्टांग योग का पूर्णता से पालन करना अनिवार्य है। मगर, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो पूर्णत्व से पालन नहीं कर सकते, उन्हें कुछ फल प्राप्त होगा ही नहीं। अष्टांग योग का यह पथ एक ऐसी धारा है, जिस पर हम जितना चलेंगे, उतना फल प्राप्त होता जाता है। जिस प्रकार यदि कोई भूखा व्यक्ति अन्न का एक दाना भी खा लेता है, तो उसकी कुछ न कुछ भूख अवश्य मिटती है और भरपेट खा लेता है, तो पूर्णता से भूख मिट जाती है। अत: इस अष्टांग योग का आप जितना पालन करते जायेंगे, उतना फल आपको प्राप्त होता जायेगा। इस पथ पर चलने के लिए ऐसा भी नहीं है कि जब आप एक अंग का पालन कर लें, तभी दूसरे में बढ़ें। आप सभी आठों अंगों को एक साथ अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा योग के आठों अंग मजबूत होते जाते हैं। ये सभी आठों अंग एक-दूसरे के पूरक हैं। इनमें प्रथम पांच अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग योग कहलाते हैं, जो स्थूल जगत् से जुड़े हुए हैं। धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग योग कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जगत् से जुड़े हुए हैं।
मानवजीवन के लिए प्रथम दो अंग यम और नियम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन दोनों के मजबूत होने पर शेष सभी अंगों पर सहज भाव से पकड़ मजबूत होती चली जाती है, चूंकि अंतिम तीन अंगों की गहराई को प्राप्त करने के लिए यम-नियम का पूर्णतया पालन करना अत्यन्त अनिवार्य है। इसके बिना समाधि की पूर्णता को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। यह अष्टांग योग वास्तव में एक शक्ति योग है। इसे जिसने कर लिया, वह शक्तिवान् बन गया और जिसने नहीं किया, वह सामान्य रह गया।
प्रथम अंग-यम
इस अंग को पांच भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का विस्तार इतना बड़ा है कि एक भाग में ही एक ग्रन्थ तैयार हो जाये। मगर, यहां पर इन भागों की मूल भावना को ही व्यक्त किया जा रहा है।
- अहिंसा- मन-वचन-कर्म के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कार्य न करना, जिससे किसी भी प्राणी, जीव-जन्तु या स्वयं का अहित हो रहा हो अथवा कष्ट पहुंच रहा हो, अर्थात् सभी के हित की और सभी के प्रति प्रेम की भावना ही सच्ची अहिंसा है। किसी दूसरे को भी हिंसा के प्रति प्रेरित नहीं करना चाहिए। अपने सामने किसी दूसरे के द्वारा हो रही ङ्क्षहसा का विरोध करना भी अहिंसा है, अर्थात् न हिंसा करें और न हिंसा होने दें। साथ ही, अपने ऊपर हो रही हिंसा को भी न सहें।
- सत्य- अपनी योग्यतानुसार मन, बुद्धि, अंत:करण व इन्द्रियों द्वारा जो सत्य देखा, सुना व समझा गया, उसे वैसा ही व्यक्त करना सत्य कहलाता है। सदा सत्य बोलें व स्वयं सत्य पर अमल करें। सत्य की ताकत सबसे बड़ी ताकत कही गई है। सत्य के फल का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। दूसरों को जो भ्रम में न डाले, धोखा न दे, वैसा ज्ञान, वैसी वाणी सत्य कहलाती है। सत्य बोलने में प्रिय हो तथा सदैव सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ सत्य ऐसे होते हैं, जहां हमें कटु बोलना पड़ता है, जैसे किसी चोर को चोर कहना, हत्यारे को हत्यारा कहना, देशद्रोही को देशद्रोही कहना आदि इन्हें कहना पूर्ण सत्य माना जाता है। मगर, हम यदि अंधे को अंधा न कहकर सूरदास कह दें, तो वह प्रिय सत्य कहा जाता है। मनुष्य को मन-वचन-कर्म से सदैव सत्य का पालन करना चाहिए।
- अस्तेय- मन-वचन-कर्म से किसी भी ऐसी चीज की इच्छा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिस पर अपना अधिकार न हो, जैसे किसी का सामान चुराकर न लेना, किसी से छलपूर्वक छीनकर, बलपूर्वक या किसी को प्रेरित करके कुछ ऐसा प्राप्त न करना, जिस पर अपना अधिकार न हो। वही अस्तेय है।
- ब्रह्मचर्य- मन-वचन-कर्म से विषय-विकारों-वासनाओं को न अपनाना ही ब्रह्मचर्य है, अर्थात् सभी कामवासनाओं पर पूर्णतया नियंत्रण का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने से मनुष्य की चेतनाशक्ति प्रभावक होती है, बल-बुद्धि-आयु में वृद्धि होती है तथा मनुष्य सत्यपथ की ओर बढऩे लगता है। गृहस्थ मनुष्य को शादी से पूर्व पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा शादी के बाद एक पतिव्रत/एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थी में रहकर भी अधिक से अधिक वासनाओं पर नियंत्रण करें और उम्र के चौथे पड़ाव में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जीवन में जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं।
- अपरिग्रह- अपने जीवन के लिए नितांत आवश्यकता से अधिक सुख-साधन का संग्रह न करना अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक दान भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ की भावना होनी चाहिए। पंचतत्त्वों से जुड़े संसाधनों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रलोभनों से हम जितने मुक्त रहेंगे, उतना ही हमारा अपरिग्रह होगा, उतना ही मन वैराग्य भाव की ओर बढ़ेगा। अपने अंदर उपयोग की भावना हो, उपभोग की नहीं।
द्वितीय अंग-नियम
जीवन किस प्रकार जिया जाये और मनुष्य की दिनचर्या कैसी हो? इसके लिए पांच नियम बताये गये हैं-
- शौच- शरीर और मन की शुद्धता व पवित्रता को ही शौच कहा गया है। इसमें नियम से नित्यप्रति शौच क्रिया आदि के लिए जाना, शरीर की शुद्धता के लिए स्नानादि करना, सत्कर्मों से उपार्जित सात्त्विक भोजन करना सम्मिलित हैं। सत्कर्मो से भी शरीर की शुद्धता होती है। मन की शुद्धता अत:करण की शुद्धता मानी जाती है। राग-द्वेष, ईष्र्या, काम-क्रोध-लोभ तथा भय का त्याग करने से अंत:करण व मन की शुद्धता होती है।
- संतोष- अपने सत्कर्मों तथा पुरुषार्थ से उपार्जित जो भी धन-संसाधन आदि प्राप्त होजायें, उनसे ही संतुष्ट रहना एवं सुख-दु:ख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सर्वदा संतुष्ट व प्रसन्नचित्त रहने का नाम संतोष है।
- तप- जीवन को सत्यपथ पर बढ़ाने के लिए मन व इन्द्रियों के संयमन एवं आत्मचेतना की प्राप्ति के लिए जप-तप-योग-ध्यान तथा व्रत-उपवास हर विपरीत परिस्थिति व सभी मौसमों सर्दी-गर्मी-बरसात में एक समान अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करने को ही तप कहा गया है।
- स्वाध्याय- ज्ञान अनुभव की प्राप्ति के लिए सत्संग, गुरुवचनों को सुनना, धर्मग्रन्थों एवं शास्त्रों का अध्ययन करना, स्तुति-स्तोत्र का पाठ करना आदि स्वाध्याय कहलाता है।
- ईश्वर प्राणिधान- मन, वाणी, कर्म के द्वारा इष्ट की भक्ति करना, उनके नाम का जप करना, उनके गुणों का गुणगान करना, स्मरण करना, कीर्तन-भजन करना व पूर्ण समर्पण भाव रखना ही सच्चे अर्थों में ईश्वर प्राणिधान है।
तृतीय अंग-आसन
आसन अनगिनत हैं। मनुष्य शरीर की हर गतिविधि व क्रियायें सब आसन ही हैं। हम जो भी दृश्यजगत् में देखते हैं, उन दृश्यों से हमें किसी न किसी आसन का बोध होता है। वैसे हमें जिस आसन पर बैठने से सुख प्राप्त हो, वह भी एक आसन है। आत्मचेतना की प्राप्ति व योग साधना में सहायक कुछ अलग-अलग आसनों का क्रम निर्धारित किया गया है। इनमें कुछ तो शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और कुछ मन को एकाग्र रखते हैं। कुछ आसनों से आत्मचेतना प्रभावक होती है। शरीर की समस्त नाडिय़ों के शोधन एवं कोशिकाओं की चैतन्यता आदि के लिए अलग-अलग आसन निर्धारित किये गये हैं। कुछ आसन व्यायाम के लिए तथा कुछ चेतना की प्राप्ति में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में मनुष्य की जो जीवनचर्या है, वह आरामपरस्त अधिक है, जिसके कारण उसके शरीर में जड़ता अधिक आ चुकी है। इसी जड़ता को दूर करने के लिए सैकड़ों प्रकार के महत्त्वपूर्ण आसन निर्धारित किये गये हैं। जड़ता के दूर होने पर ही धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ा जा सकता है, जिनमें से कुछ ऐसे आसन सिद्ध किये जा सकते हैं, जिनमें अधिक से अधिक देर तक बैठकर ध्यान-साधना की जा सकती है। इस पुस्तक में सभी आवश्यक महत्त्वपूर्ण आसन आगे दिए गये हैं।
नोट- आसन-प्राणायाम प्रारम्भ करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि उन्हें किस क्रम से प्रारम्भ किया जाय? शरीर की शिथिलता और चैतन्यता के आधार पर कुछ सावधानियां आवश्यक होती हैं। यहां पर एक ऐसे क्रम की जानकारी दी जा रही है, जिससे करने पर शरीर को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि नित्यप्रति आसनों के साथ ही कुछ व्यायाम और प्राणायाम भी कर लिये जाते हैं। चूंकि हमारा शरीर सामान्यत: हमेशा चैतन्य नहीं रहता, इसलिए पहले कुछ ऐसे आसन कर लिये जाते हैं, जिससे शरीर में स्फूर्ति, लचीलापन और चैतन्यता आजाय और शारीरिक जड़ता दूर हो जाये। फिर हम कठिन आसन भी करते हैं, तो आसानी से बन जाते हैं। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार आसनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं और समयानुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं।
चतुर्थ अंग– प्राणायाम
प्राण ही जीवन है, प्राण ही चेतना है, प्राण ही शक्ति है, प्राण ही सत्य है, प्राण ही औषधि है तथा प्राण ही अंधकार से प्रकाश की ओर लेजाने वाला सशक्त माध्यम है। हमारा शरीर प्राणचेतना से ही संचालित है। प्राणों के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। हमारे शरीर की सभी क्रियायें प्राण के द्वारा ही संचालित हैं।
प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के सभी सातों चक्रों को चेतना प्रदान करके तथा अपना पूर्ण आत्मोत्थान करके अपनी दिव्य शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा ही ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। हमारे शरीर में पंचप्राणों के द्वारा ही सभी क्रियायें संचालित होती हैं। प्राणायाम के द्वारा ही शरीर के पंचकोषों को जाना और समझा जा सकता है।
प्राणायाम एक बहुत व्यापक विषय है। समय के साथ प्राणायाम के विषय में एक अलग पुस्तक तैयार करके जनहित में प्रदान की जायेगी। इस शक्तियोग पुस्तक के अन्तर्गत प्राणायाम के विषय में कुछ प्रारम्भिक महत्त्वपूर्ण प्राणायाम व उन्हें करने की विधि का ज्ञान दिया जा रहा है।
प्राणायाम का अर्थ केवल श्वासों को नियंत्रित करना और उन्हें रोकना ही नहीं है। साधक जब इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मैं एक अजर-अमर-अविनाशी आत्मा हूँ तथा प्राण ही एक ऐसा माध्यम है, जिससे मैं अपने स्वरूप को जान सकता हूँ, अपनी आत्मा को जान सकता हूँ, तब वह अपने मन को प्राणचेतना में एकाग्र करके अपने आपको प्राण ही समझने का प्रयास करता है। प्राणायाम करते-करते मन सहज एकाग्र होने लगता है। इससे हमारी अंतरकोशिकाएं चैतन्य होजाती हैं।
प्राण के प्रथम चरण में पूरक, कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक के क्रम को समझना व प्रारम्भ करना नितांत आवश्यक है। सहज प्राणायाम में यह चार क्रियायें ही होती हैं।
प्राणायाम की सम्पूर्ण जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें
पंचम अंग–प्रत्याहार
प्रत्याहार अष्टांग योग का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह बहिरंग और अंतरंग योग को जोड़ता है, जिसमें हम यम-नियम-आसन का अभ्यास करते हुए, अपने मन को इन्द्रियों के भोग से अलग करने में सफल होते हैं। यहां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के प्रभावों से मन अलग हटकर चित्त के साथ अंतरंग योग की तरफ या आत्मतत्व की सहज शक्ति की तरफ आकर्षित होता है तथा अन्नमय कोष से हटकर हमारा प्राणमय कोष से सम्बन्ध स्थापित होता है। यहां हमारी इन्द्रियां अपने सहज स्वभाव को त्यागकर मन के साथ चित्त की एकाग्रता की ओर आकर्षित होती हैं। इसी प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं, जहां से हम धारणा की ओर बढ़ते हैं।
षष्ठ अंग– धारणा
धारणा का तात्पर्य है, किसी चीज़ को धारण करना। अष्टांग योग में धारणा पूर्णतया अंतरंग योग का विषय है, अर्थात् तमोगुण, रजोगुण से हटकर सतोगुण को धारण करना, अर्थात् उस अवस्था की ओर बढऩा, जहां हमारा सत्य से एकाकार होना प्रारम्भ होता है। सामान्यतया हम सदैव भौतिक जगत् की मान्यताओं रीति-रिवाजों, विचारों एवं परम्पराओं को ही धारण किए रहते हैं। इन समस्त विचारों एवं परम्पराओं से बिल्कुल अलग हटकर अंतरंग की सत्यता को धारण करना, उसके प्रति आकर्षित होना अर्थात् एक पूरी विचारधारा से अलग हटकर चेतना की विचारधारा को धारण करना ही धारणा है, जो सही अर्थों में एक नवीन जन्म कहलाता है। यहां हम सभी पूर्वाग्रहों को त्यागकर अपने चित्त में किसी न किसी सत्य के बिन्दु सप्तचक्रों या ऊर्जा को धारण करने की दिशा में बढ़ जाते हैं और हम पूर्ण निर्विकार होकर सत्य को धारण करते हैं, अर्थात् सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारी धारणा का मूल अभिप्राय है।
धारणा के बाद ही सही मायने में मनुष्य की मुक्तिपथ की यात्रा प्रारम्भ होती है, जहां हमें हर पल सत्य का सान्निध्य प्राप्त होता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि इस सत्य को स्वीकार कर लेती है कि दृश्य से परे अदृश्य सत्ता ही पूर्ण है, परिपूर्ण है। यहां हमें ज्ञान होता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा हूँ और मेरी विराट्ता व्यापक है, जिसमें आनन्द ही आनन्द है। मगर, साधक को इस बिन्दु पर बहुत सजग होने की आवश्यकता होती है। कई बार कुछ साधक उस सत्य को जानकर भी उसे धारण करके अपनी ही धारणा बना लेते हैं और भौतिक जगत् के बीच छोटी-मोटी अपनी सत्यता की विचारधारा समाज में धर्मगुरु बनकर प्रवाहित करने लगते हैं, जब कि यह विचारधारा पूर्ण नहीं होती। साधक को धारणा के बाद अपनी कुण्डलिनी शक्ति जागरण की लम्बी यात्रा की ओर बढऩा पड़ता है। ध्यान एवं समाधि की सीढिय़ों को पार करते हुए, सत्य से एकाकार करना ही हमारी सच्ची मुक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्चा आनन्द होता है, जहां पर कोई भी पतन नहीं होता।
सप्तम अंग–ध्यान
ध्यान का तात्पर्य है कि किसी एक चीज, एक बिन्दु या एक ऐसी विचारधारा पर एकाग्रता करना, जिसे मन और बुद्धि धारण कर रहे हों। यह बाह्य क्रम की एक सहज अवस्था होती है। हम प्राय: देखते हैं कि कई बार साधारण इन्सानों का भी ध्यान किसी न किसी चीज़ पर लग जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से खो जाता है, एकाग्र हो जाता है या किसी एक चीज़ पर उसकी ऐसी लगन लग जाती है, जिसमें वह अन्य सभी बातों को भूल जाता है। अनेकों लोग कई कार्यों को बड़े ध्यान के साथ करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, उसे भी ध्यान कहते है। मगर, वह सभी ध्यान हमारे सुख-दु:ख, लाभ-हानि इन्द्रियों के सहज स्वभाव से प्रभावित होता रहता है। हम यहाँ पर उस ध्यान की अवस्था की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सत्य का बोध होता है तथा स्वयं का बोध होता है कि मैं कौन हूँ। वस्तुत: कुण्डलिनी चेतना की ऊर्जा का साक्षात्कार या आत्मसाक्षात्कार की प्रथम अवस्था ही ध्यान है, जो क्रमिक रूप से प्राप्त होता है। जितना हम यम-नियमों का ढृढ़ता से पालन करते हैं, उतना हमारे शरीर का संतुलन बनने लगता है, आसन में दृढ़ता आने लगती है, उतना ही हमारा प्राणतत्व सक्रिय होने लगता है और उतनी ही हमारी पकड़ प्राणों पर मजबूत होने लगती है। जितना हमारे प्राण चैतन्य रहेंगे, प्राणचेतना सुचारु रूप से कार्य करेगी, उतना ही हमारा प्रत्याहार सधने लगेगा तथा हम बाह्य इन्द्रियों को अपने वशीभूत करने में सफल होने लगेंगे। इससे हमारा मन सतोगुणी होकर सत्य की तरंगों की ओर आकर्षित होने लगता है और हमारी बुद्धि हमें चित्त की एक ऐसी अवस्था की ओर लेजाती है, जहाँ हम अंतरंग योग में पहुँचकर सत्य को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। हमारे मन व बुद्धि पर आत्मचेतना की तरंगों का आकर्षण होने लगता है और हमें अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। हम अपने समस्त भय-शोक, लाभ-हानि से ऊपर उठकर उस अवस्था का स्पर्श करने लगते हैं, जिसे आत्मसाक्षात्कार कहते हैं। यहाँ हम सत्य को जिस रूप में धारण करते हैं, वहीं पर हमारा चित्त एकाग्र होने लगता है। हम एक चेतना के आकर्षण में बंध जाते हैं, अर्थात् ध्यान लगाना नहीं पड़ता। जहाँ ध्यान स्वयं लगने लगे, वहीं सच्चा आत्मसाक्षात्कार का प्रारम्भ है। यहाँ से हम अपनी कुण्डलिनीचक्रों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उसी अवस्था को ध्यान कहते हैं, जहाँ अन्य कोई भाव-विचार स्पर्श नहीं करते। यद्यपि ध्यान की अलग-अलग कई अवस्थायें होती हैं, मगर यहाँ पर ध्यान के प्रारम्भिक स्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है।
ध्यान में जाने के लिये हमारे शरीर के सात चक्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण चक्र आज्ञाचक्र है, जिस पर ध्यान लगाकर हम भौतिक जगत् की भी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं व अंतरंग योग में उतरकर आत्मसाक्षात्कार कर सकते हैं। आज्ञाचक्र को राजाचक्र कहा गया है। यह चक्र हमारी बुद्धि का, ज्ञान का चक्र कहा जाता है। अत: नित्यप्रति आज्ञाचक्र पर ध्यान लगाने से क्रमश: ध्यान की अवस्था ढृढ़ होते-होते आत्मसाक्षात्कार होजाता है।
ध्यान की गहराई में डूबने के लिये साधक को अपने तन-मन और बुद्धि को निर्मल और पवित्र बनाना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह अंतरंग योग में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा उसका ध्यान बाह्य जगत् के कुछ छोटे-मोटे लाभों तक सीमित रह जाता है। मन की कुछ संतुष्टि, कुछ अनुभूतियों को ही साधक प्राय: अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेता है और इसी से कई बार उसका पतन शुरू होजाता है। अंतरंग योग की गहराई में प्रवेश करने के लिये, आत्मसाक्षात्कार के लिये एक चेतनावान् अनुभवी, सिद्ध, पूर्ण योगी गुरु की आवश्यकता होती है। वही अपने आशीर्वाद व मार्गदर्शन से साधक को गहराई या उच्चता की ओर लेजा सकता है। ध्यान की गहराई मे डूबने के लिये स्थान, आसन एवं वातावरण अत्यंत मायने रखते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं, तो हमारे मन और बुद्धि आंशिक रूप से अपना कार्य करते रहते हैं। कई बार कुछ क्षण के लिये हमारा ध्यान लगेगा और फिर छूट जायेगा। कुछ क्षण हमें पूर्ण सत्य की अनुभूति होगी कि मैं एक अलौकिक दिव्यता से जुड़ रहा हूँ, जो मेरे अंदर ही समाहित है। मगर, प्रारम्भ में हम बहुत समय तक उसमें डूबकर नहीं रह सकते। धीरे-धीरे ही हमारे शरीर की पात्रता बढ़ती है। जितना हमारी सुषुम्ना नाड़ी के चक्रों की चैतन्यता बढ़ती है, उतना ही हमको ध्यान में सत्य का सान्निध्य प्राप्त होता है। एक प्रबल लगन, निष्ठा, विश्वास व समर्पण हमें धीरे-धीरे ध्यान की गहराई में ले जाता है और हमारी ध्यान में पकड़ पूर्ण होने लगती है।
पात्रता होने के बावजूद ध्यान में बैठने पर इन्द्रियाँ आंशिक रूप से मन को कई बार कुछ क्षणों के लिये बाहर की ओर लेजाती हैं। उस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। हम किसी ऐसे चिंतन पर मन को न लेजायें, जहाँ डर हो या खौफ हो। सामान्य अवस्था में हम चाहे जो भी सोचते रहें, हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। कई बार लोग आँख बंद करके निरर्थक बातों को सोचते रहते हैं, मगर उससे उन्हें समय की बर्बादी के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्षति होने का भय नहीं रहता। मगर, जब अंतरंग योग के ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो बहुत सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वास्तव में हम प्राणशक्ति के माध्यम से स्थूल शरीर के भान से अलग होते हैं, जहाँ हमें अपने स्थूल शरीर की क्षमताओं का भान समाप्त सा होने लगता है। उस समय हमारे मन की अवस्था बहुत निर्बल और कमजोर होती है। उन क्षणों पर यदि आप का ध्यान ऐसी बातों पर चला जाये कि जैसे ऊँचाई से ढलान की भूमि पर उतर रहे हैं, तो उस समय आपका ध्यान केवल छूटता नहीं हैं, बल्कि एक झटका सा लगता है फिसलकर गिरने का। और, इस झटके से ध्यान छूट जायेगा। इस तरह के विचारों पर जब हमारा थोड़ा सा भी मन चला जाता है, तो उस समय हमारे स्थूल की क्षमता शून्यवत् होती है। उस समय हमारे शरीर की अवस्था छोटे शिशु के समान होजाती है, जिसने केवल अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। वह बहुत सम्भलकर धीरे-धीरे चल पाता है। उस बच्चे की भी वही अवस्था होती है। यदि उसे ऊँची-पतली मेड़ पर खड़ाकर दिया जाये, तो डगमगाकर गिर जायेगा। वही हमारी मन:स्थिति ध्यान के समय होती है कि ऐसे चिन्तनों से कई बार मन-मस्तिष्क पर तीव्र झटके लग जाते हैं।
यदि शारीरिक व मानसिक मजबूती न हो तथा गुरु और इष्ट की कृपा न हो, तो कई बार साधक मानसिक असंतुलन का शिकार भी होजाता है। इसलिये सजगता बहुत आवश्यक है। ध्यान की अवस्था ही एक ऐसी अवस्था होती है, जो हमें सत्य से जोड़ती है। इस अवस्था में साधक का संतुलन बहुत ही आवश्यक होता है। साधक को ऐसे ऊँचे आसन पर बैठकर ध्यान नहीं लगाना चाहिये, जहाँ पर गिरकर चोट लगने का डर हो। अन्यथा, यह मानसिक एहसास भी साधक को ध्यान की गहराई में जाने पर भय पैदा करता है। ये सभी बिन्दु बहुत ही विस्तार एवं अनुभव के हैं कि हम ध्यान की किन अवस्थाओं में किस तरह के विचार बनायें? जीवन का संतुलन कैसा हो? इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय यहाँ पर बहुत संक्षिप्त सा चिंतन दिया गया है। भविष्य में ध्यान की सभी अवस्थाओं में मार्गदर्शन के लिये अलग से एक पुस्तक तैयार करके साधकों को उपलब्ध कराई जायेगी। अंतरंग योग का ध्यान सहज नहीं है। चूंकि इसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में प्रवेश करते हैं, अत: संतुलन ही हमारा मूल सहारा बनता है। अत: ऐसी अवस्था के साधक गुरु मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करें।
अष्टम अंग–समाधि
ध्यान की पराकाष्ठा का दूसरा नाम समाधि ही है। यह एक ऐसी अवस्था है, जहां पर हम स्वयं के सत्य पर केन्द्रित होकर आत्मसाक्षात्कार की दिशा में स्थिर हो जाते हैं। ध्यान में हमें आंशिक रूप से इस चीज़ का भान बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। किस तरह कर रहा हूँ, किस माध्यम से कर रहा हूँ और किसका कर रहा हूँ? अर्थात् कर्ता, क्रिया और कर्म का भान बना रहता है। मगर, समाधि एक ऐसी अवस्था है, जहां साधक, साधन और साध्य एक रूप होजाते हैं, अर्थात् आत्मस्वरूप होजाते हैं।
समाधि की प्रारम्भिक अवस्था को शून्यता की अवस्था भी कहा गया है- एक ऐसी न्यूट्रल अवस्था, जहां पर हम अपनी इन्द्रियों, मन और बुद्धि के सभी क्रियात्मक पक्षों के भान को ही भूल जाते हैं। समाधि वहीं से प्रारम्भ होती है, जो हमारी पूर्ण आत्मसाक्षात्कार की यात्रा है और उसमें भी अलग-अलग कई अवस्थायें हैं। मगर, यहां पर साधकों को इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि समाधि की अवस्था में भी सबीज और निर्बीज समाधि होती है। जब हम निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, तो वही हमारी पूर्ण मुक्ति की अवस्था होती है, जहां से हमारा पतन नहीं होता।
समाधिस्थ सिद्धसाधक को भी बहुत संतुलित जीवन जीना चाहिए। उसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं समाधिस्थ सिद्धसाधक हूँ, तो मैं चाहे जैसा जीवन जिऊँ, समाधि पर मेरी पकड़ बनी रहेगी! चूंकि कोई भी साधक हमेशा समाधि में नहीं रहता, उसे सामाजिक जीवन जीना पड़ता है, इसलिए उसे अपनी सद्बुद्धि के द्वारा हर अच्छे-बुरे कर्म का निर्णय करके सदैव सन्मार्ग पर ही चलना चाहिए, अन्यथा समाधि प्राप्त करने की क्षमताएं कब नष्ट हो जायें, कुछ कहा नहीं जा सकता। अत: यदि सत्य से जुड़े रहना है, तो सत्यपथ पर चलकर सत्कर्म करना होगा। जो उच्चकोटि के मुक्तिपथ के अभिलाषी साधक होते हैं, वे अधिकांशतया लम्बे समय तक समाधिस्थ रहते हैं, मुक्तिपथ ही उनकी मात्र यात्रा होती है और समाज से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। जब वे पूर्णत्व से अपनी प्रकृतिसत्ता से एकाकार कर लेते हैं, उसी के बाद कहा जा सकता है कि फिर उनका कभी भी पतन नहीं होता।

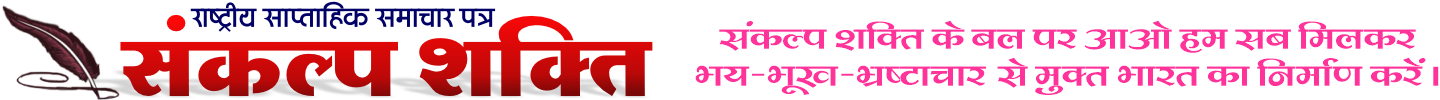




























 Views Today : 11
Views Today : 11 Views Last 7 days : 324
Views Last 7 days : 324 Views Last 30 days : 1233
Views Last 30 days : 1233 Views This Year : 59023
Views This Year : 59023 Total views : 88568
Total views : 88568 Who's Online : 0
Who's Online : 0 Your IP Address : 18.118.255.51
Your IP Address : 18.118.255.51